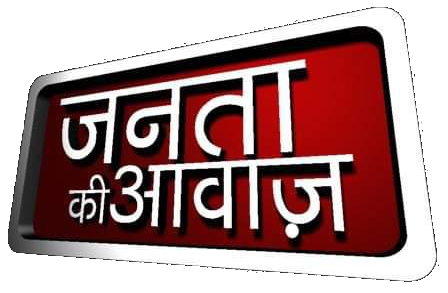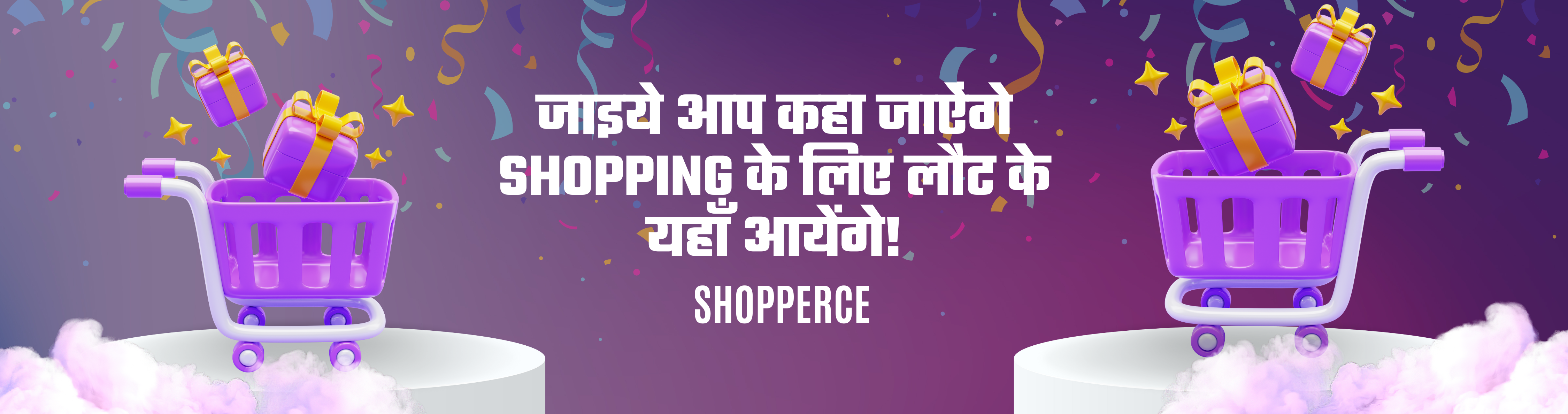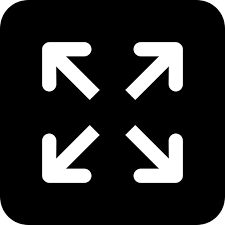संवादहीनता से अवसाद की तरफ बढ़ता बचपन
BY Anonymous20 Jan 2018 10:40 AM GMT

X
Anonymous20 Jan 2018 10:40 AM GMT
डॉ. उपेन्द्रमणि त्रिपाठी
मीडिया रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में बाल अपराधों में 62% बृद्धि हुई, जिसमे 16 से 18 आयु वर्ग किशोरों की संलिप्तता सर्वाधिक है।बच्चों से संवादहीनता, संस्कारविहीन शिक्षा, और प्रतिस्पर्धा में अपेक्षा के निरन्तर दबाव के चलते अवसाद जैसी मनःस्थितियां उनमें आपराधिक वृत्ति पनपने के संकेत हैं, समय रहते सुधारने के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि आज आने वाले कल का संकेत है।
"छुट्टी के लिए 11 वर्षीय छात्रा ने कक्षा एक के छात्र को चाकू मारा"... "विद्यालय के शौचालय में छात्र की हत्या"...विद्यालय की छत से कूद कर छात्र की मृत्यु"...समाचारों के यह शीर्षक किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर देने वाले हैं , क्योंकि यह मात्र अपराध या दुर्घटना नहीं ,आज के समाज की इस मौलिक इकाई से तरुणाई में निर्मित होने वाले समाज की तस्वीर की कल्पना करें तो रक्त का रंग स्याह हो जाएगा।
बचपन का मन निर्मल, निश्छल और चंचल होना चाहिए तो फिर उसमें यह मलीनता,ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति, कैसे और कब घर कर गयी कि उसकी चंचलता षड्यंत्र कर उसे साकार करने लगे। इस दृष्टिकोण से यह भविष्य के लिए सचेत हो जाने का स्पष्ट संकेत है यदि अब भी हमारी चेतना नही जागी तो पीढ़ियों के अपराधी होने से कोई नही बचा सकता।
बच्चे अपराधी हैं ऐसा बिल्कुल नहीं , किन्तु इस अवस्था मे उनसे ऐसे अपराध हो जाएं तो यह निश्चित ही इस बात का संकेत है कि उनके मस्तिष्क में विचारों, कल्पनाओं की गति, उनकी आयु की तुलना में तीव्र है, और यही असामान्य कारण है। निर्मित होती इन परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक आकलन और उनके उपाय करना जरूरी है। चिकित्सकीय दृष्टि से ऐसे व्यवहार का कारण अवसाद का पाया जाना होता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक तथ्य उल्लेखनीय है कि अधिकांशतः ऐसी घटनाएं ज्यादातर बड़े शहरों, और उच्चसुविधा सम्पन्न मंहगी फीस वाले प्राइवेट विद्यालयों में ही हुईं, अर्थात ये बच्चे उन परिवारों से सम्बंधित हैं जहां इनकी सुख सुविधा के लिए कोई कमी नहीं।
....तो क्या हमारी पीढ़ी में बच्चे भी अवसाद से प्रभावित होने लगे हैं।
विश्वसनीय तो नहीं किन्तु इस प्रासंगिक प्रश्न का एक ही उत्तर है शायद.. हां..हमारे बच्चे 8 से 15 वर्ष की आयु के साथ अवसाद की मनोवृत्ति की तरफ बढ़ रहे है।
बच्चे भी इसी समाज की मौलिक इकाई हैं , उनकी भी अपनी अभिरुचियाँ हैं, अभिव्यक्ति है, योग्यता है, अपेक्षाएं हैं, क्षमताएं हैं किन्तु यह तर्क हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके प्रति दायित्वों का निर्वहन करने हेतु आधुनिक भौतिकवादी ,अर्थयुग में समय से प्रतिस्पर्धी माता पिता के पास बच्चों को देने के लिए सुख ,सुविधाएं ,संसाधन तो बहुत हैं , कुछ नही है तो बस समय।
यूँ भी समझ सकते हैं कि इस तकनीकी युग मे बच्चों के हाथ मे मोबाइल , लैपटॉप ने उन्हें समय से पहले दुनिया की उन तमाम जानकारियो से जुड़ने का अवसर दे दिया जिसके लिए उनकी अवस्था और मानसिक ग्राहिता उपयुक्त या परिपक्व नहीं कही जा सकती।
कम समय मे दुनिया से जुड़ने का महत्वपूर्ण कारण हमारा सांस्कृतिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों से अलगाव भी है । पहले संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों ने ली, फिर परिवारों का यह बंटवारा पीढ़ियों की खाई से बढ़ गया क्योंकि बुजुर्ग अपने घर मे बेटा बहू अपार्टमेंट में और बच्चे या तो आया की जिम्मेदारी में या पालनाघर में अथवा हॉस्टल में। इसका सबसे नकारात्मक दुष्परिणाम दिखने लगा है कि जीवनकौशल का जो पाठ बच्चे दादा ,दादी ,नाना,नानी से परिवार में सीख लिया करते थे आज वे रिश्तों की इस मधुरता ,नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक मूल्यों से अपरिचित होते जा रहे हैं और उनकी मनोदशा अनियंत्रित, किन्तु स्वभावतः कल्पित स्वरूप को वास्तविक सत्य के रूप में स्वीकार करने लगती है, जहां चिंतन, मंथन, धैर्य, विवेक का प्रयोग क्रमशः सीमित होने लगता है और आचरण व्यवहार में स्वच्छंदता आती जाती है। परिवार के बाद विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण का मंदिर हुआ करते थे किंतु वर्तमान में अब यह स्वरूप भी व्यवसायिक होता गया, यह केवल अक्षर ज्ञान और पाठ्यक्रम पूरा कराने की कार्यशाला भर रह गए लगते है जहां संस्कृति और नैतिक आचरण को रूढ़िवादी मानकर धीरे धीरे त्याग दिया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमो में बच्चों के प्रतिभाग की जगह कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ने ले ली है। बालमन पर माता पिता शिक्षकों की अपेक्षाएं उनको लक्ष्य केंद्रित परफॉर्मेंस के लिए थोप दी जाने लगी हैं।
बच्चों को लेकर देखा जाए तो ये अपेक्षाएं किसी "अर्थतंत्र के विकसित मॉडल" की तरह नजर आती हैं जहां बचपन हमारे लिए उस खिलौने जैसा होता है जिसमे हम रिमोट का जैसा बटन दबाएं वह वैसा ही प्रदर्शन करने लगे। बच्चों की स्वीकार्यता जाने बिना उनपर अपेक्षाएं और प्रतिस्पर्धाएं थोप दी जाती हैं यह उनके मन मस्तिष्क और भावनाओं का दमन करती है। जिसकी प्रतिक्रिया में उनमे कई तरह के मानसिक और शारीरिक लक्षण उभरते हैं जिनकी पहचान समय समय पर जागरूक माता पिता या शिक्षक कर सकते हैं। किन्तु ऐसा होता तो बाल अपराध के आंकड़े यूँ न होते।
संवादहीनता से पनपता बचपन मे अवसाद
इस पूरे विचार प्रवाह में बच्चों को इस अवसाद की तरफ ले जाती मनोवृत्ति के उद्भव का मूलकारण है संवादहीनता।
संवाद हीनता प्रमुख रूप से तीन स्तरों पर देखी जा सकती है मातापिता और बच्चों के बीच, बच्चे और शिक्षकों के बीच, और शिक्षक व माता पिता के बीच।
संवादहीनता के कारण बच्चे अपने मन की बातें अपने ही माता पिता से खुलकर कह पाने का अवसर नहीं पाते। जिससे माता पिता को अपने बच्चे के व्यवहार, विचार, पसन्द, नापसन्द ,अभिरुचि आदि का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता। विद्यालय में शिक्षक छात्रों के बीच परस्पर संवाद कम ही हो पाता है जिससे छात्रों की जिज्ञासाओं को उचित समाधान नही मिल पाता साथ ही शिक्षक बच्चे की अभिरुचियों या क्षमताओं योग्यताओं का वास्तविक आकलन नही कर पाते,और इसतरह शिक्षक मातापिता की संवादहीनता केवल रिपोर्टकार्ड पर हस्ताक्षर तक सीमित हो जाती है।
कैसे पहचाने
बच्चे का जिज्ञासु मन अपराध की तरफ किसी प्रेरणा से ही उन्मुख हो सकता है, इसलिए उसके व्यवहार का आकलन जरूरी है। मानसिक रूप से किसी बात पर जिद, उत्साह चंचलता की कमी, चिड़चिड़ापन, सामान्यतः शारीरिक लक्षणों के रूप में भूख में कमी, वजन परिवर्तन, नींद का पैटर्न बदलना, टीवी या मोबाइल पर लम्बा समय व्यतीत करना, बातचीत के तरीके, एकाग्रता में कमी, उतावला पन या आलस्य, आलस्य, यादाश्त ,पाचन तंत्र की गड़बड़ी, सक्रियता कम होने लगे तो आपके बच्चे को चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है।
क्या कहता है होम्योपैथी का विज्ञान
होम्योपैथी के मनोदर्शन और विज्ञान के अनुसार यह बच्चे के अंदर तेजी से सोरा मायज्म को प्रभावित करता है और सायकोटिक अवस्था मे प्रवर्तित होते हुए सिफिलिटक स्वरूप तक विकसित हो सकता है इसलिए बच्चे के व्यक्तित्व में तीव्र मानसिक हलचलें उसे बेहद कल्पनाशील बना देती हैं जिससे वह एक काल्पनिक पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है और क्षमतानुरूप अवसर मिलने पर बालस्वभाव वश वह उसे क्रियान्वित कर डालता है, क्योंकि उसे यह अपराध नहीं सबकुछ एक फ़िल्म की गढ़ी कहानी के फिल्मांकन जैसी अनुभूति देता होगा। संभवतः इतने अवस्था के सापेक्ष यह मनोवृत्ति के परिवर्तन की यह गति तीव्र होती है जिसे ग्रहण कर पाने या समझ पाने की क्षमता बचपन मे नही होती।
इसी बचपन की आधारशिला पर विकसित होने वाला तरुण और युवा ...उसकी दशा दिशा क्या होगी वह कितना अधीर होगा और तब समाज का स्वरूप क्या होगा ? इसलिए हमे इसी समय सचेत होने की आवश्यकता है।
क्या करना चाहिए
सबसे प्रथम आवश्यकता है कि माता पिता , परिवार, और शिक्षक या विद्यालयों सभी स्तरों पर परस्पर और स्वस्थ संवाद को व्यक्तिगत, व सामूहिक वार्ता के रूप में स्थापित और समृद्ध किया जाए।
विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक आकलन की तकनीक अपनाते हुए छात्र संसद के गठन के माध्यम से माता पिता ,छात्र , शिक्षकों तीनो में अलग अलग व एक साथ जिज्ञासाओं के समाधान के सत्र आयोजित किये जाने चाहिए।
बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं थोपने की बजाय उनकी अपेक्षाओं , क्षमताओं ,योग्यताओं , अभिरुचियों और अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देकर सामंजस्य पूर्ण तरीके से सांस्कृतिक , नैतिक जीवनमूल्यों एवं आदर्शों से परिचित कराया जाना चाहिए। प्रार्थनाओं से जुड़कर ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाये, इससे उनमे नम्रता एकाग्रता , विश्वास, आशावान और धैर्य का गुण विकसित होता है।
Next Story