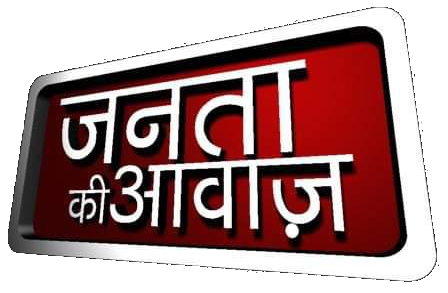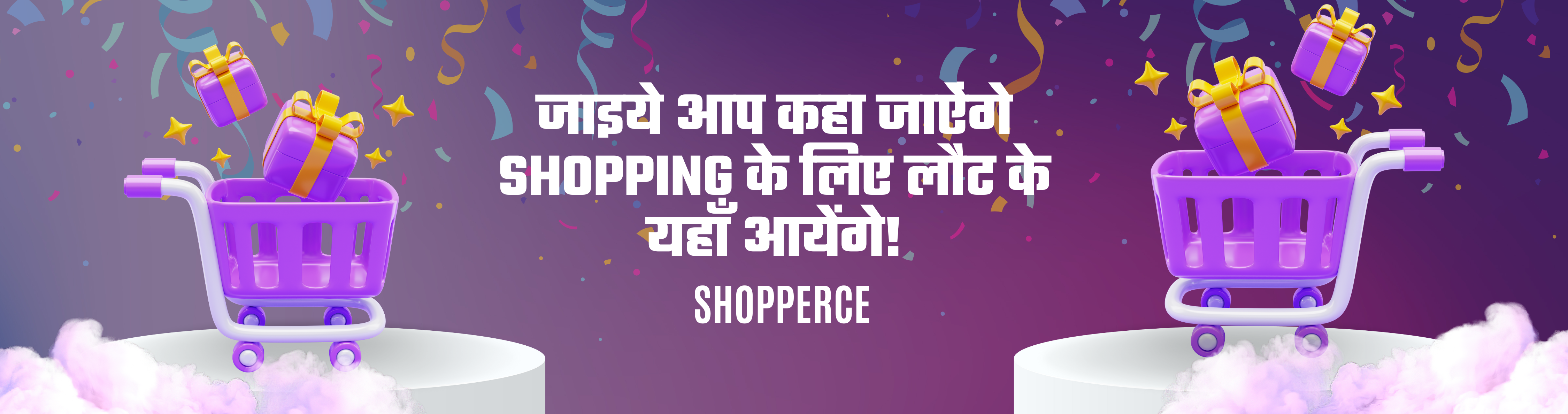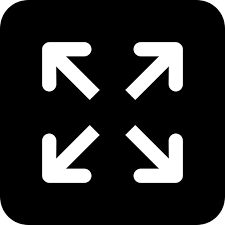कार्टन या पैकेट्स के निस्तारण की समस्या और पर्यावरण संरक्षण – प्रोफेसर (डॉ.) योगेन्द्र यादव

प्रगति और आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में हमने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। जिससे पर्यावरण को इतना नुकसान हुआ कि पृथ्वी पर मानव जीवन बचेगा कि नहीं, ऐसा संकट उत्पन्न हो गया । पिछले कई महीने से पूरी दुनिया कोरेना महामारी से पृथ्वी पर जीवन बचाने के जद्दोजहद में लगी हुई है। एक निर्जीव वायरस कोविड – 19 ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अपनी प्रगतिशीलता और आधुनिकता का जो हम दंभ भरते रहे हैं, उसकी पूरी पोल खोल कर रख दी है । तीन महीने से अधिक बीत गए, पूरी दुनिया उसकी वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं, जिसमें अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है। जो लोग उससे संक्रमित हो रहे हैं, उनके इलाज के नाम पर हम उन्हें कोरेंटाइन कर रहे हैं। अंदाज से कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई कम हो सके, उसका बुखार उतर सके और 14 दिन की अवधि वह पूरी कर ले। ऐसा पाया गया है कि लगभग 14 दिन कोरेंटाइन होने पर कोरेना संक्रमण समाप्त हो जाता है ।
जिस आधुनिकता के दौर में हम जी रहे हैं। बाजारवाद और चमक ने जिस तरह से हमारे मनोमस्तिष्क पर कब्जा जमा लिया है । उसी वजह से कोई भी उत्पाद हो, उसकी पैकिंग पर सभी कंपनियाँ अधिक ध्यान देती हैं। सीमित मात्रा और लंबी अवधि तक काम आने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग तो ठीक है। उसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, कि कोई समस्या खड़ी हो सके। लेकिन ऐसी वस्तुएं, जैसे दूध का पैकेट, गुटखा या अधिक संख्या में और अधिकांश लोगों द्वारा जो उत्पाद उपयोग में लाये जाते हैं। उनकी पैकेटिंग एक समस्या के रूप में उभर कर आए हैं । प्लास्टिक युग में प्रवेश करते समय हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसका निस्तारण कल एक समस्या बन जाएगा । किसी शहर या छोटे से नगर से निकलने वाले कूड़े की मात्रा अगर आप देख लें, और उसे एक ही जगह कुछ दिन डालें, तो कूड़ों का एक पहाड़ तैयार हो जाएगा ।
आज शहरों से लेकर गावों तक इस प्रकार के कूड़े एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं । ज़्यादातर प्लास्टिक के पैकेट्स होने के कारण उनका निस्तारण भी सहज और सरल नहीं है। यह न गलते हैं, न सड़ते हैं। जल्द ही इस समस्या से प्रशासन से लेकर सरकारें सचेत हुई। पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस समस्या को उठाया और उससे होने वाले दीर्घजीवी हानि की तरफ सरकार और प्रशासन का ध्यान खीचा । इसके बाद इस दिशा में जन जागरूकता अभियान चलाये गए। लोग सजग हुए। सरकारों ने बन्दिशें लगाई। कंपनियों ने ऐसे पैकेट्स या कार्टन में समान की पैकेजिंग करना शुरू कर दिया। उपयोग होने के बाद जिसका डिस्पोजल किया जा सके ।
पर्यावरण विभाग, सरकारों और उनके विभागों द्वारा की गई सख्ती और जन-जागरूकता के कारण इस दिशा में प्रगति हुई है। एक ओर जहां लोग पालीथीन का कम उपयोग करने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकांश कंपनियाँ भी ऐसे कार्टन या पैकेट्स बनाने लगी हैं, जिनका आसानी से डिस्पोजल किया जा सके ।
अपनी पैकेजिंग के जरिए लोगों तक सुरक्षित उत्पाद पहुंचा कर पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। कंपनियाँ उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त कार्टन का निर्माण इस प्रकार करती हैं, जिससे उसके हर भाग को रीसाइकिल किया जा सके। इससे कचरे के निपटान में भी मदद मिलती है। इनका काम केवल प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक ही अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी उसमें जोड़ लिया गया है । इसके लिए ये कंपनियाँ एसेप्टिक पैकेजिंग तकनीक अपना रही हैं, जो उत्पाद को बिना रेफ्रीजिरेशन और प्रिजर्वेटिव्स के सुरक्षित रख सके। एसेप्टिक पैकेजिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होती। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद ये पैकेट्स देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं । इसमें बड़े-छोटे शहर के अलावा दूरदराज के इलाके भी शामिल हैं। इन पैकेट्स को देश की की सुदूर सीमाओं तक भी पहुंचाया जाता है, जहां हमारी सेना तैनात है।
कोरना महामारी के बाद वर्तमान परिस्थिति हमें विवश कर रही है कि उत्पाद सुरक्षा के सभी मापदंड़ों का सख्ती से पालन किया जाए। इतने स्पष्ट रूप से प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक उत्पाद सुरक्षा की अहमियत शायद ही इसके पहले महसूस की गयी हो। इससे उत्पाद की बरबादी भी नहीं होती है, और वह उपभोक्ता के हाथों तक सुरक्षित पहुंचता है ।
कोरेना संक्रमण जैसी महामारी, जिसके सामने पूरी दुनिया लाचार दिखाई पड़ रही है। पूरी मेडिकल साइंस को जिसने फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। कोविड – 19 को समाप्त करने और उससे संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने के लिए अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है । इससे सभी को एक सीख मिली है, सभी ने एक सबक सीखा है तथा प्रकृति की ओर से मिली उस चेतावनी को महसूस किया है कि अगर हम पर्यावरण को लेकर संजीदा नहीं हुए, तो वह दिन दूर नहीं, जब पृथ्वी से मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा ।
कोरेना संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉक डाउन किया है, पर्यावरण के संदर्भ में उसके परिणाम सभी को दिखाई पड़ने लगे हैं । देश की सभी नदियों के जल की शुद्धता और गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। गाड़ियों और कल-कारखाने न चलने से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। श्वास संबंधी रोग कम हुए हैं । इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन यह हुआ। इस कारण हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और प्रदूषण न फैले, इस कारण जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना होगा। चाहे आम नागरिक हो, उपभोक्ता हो या कल-कारखाने हों। सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए कि दिशा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।
लेकिन हम सभी को इस सच को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि सिर्फ रीसाइक्लिंग तकनीक या उत्पाद ही पर्यावरण समस्या का हल नहीं है। कंपनियों को यह भी सोचना होगा कि जो प्रोडक्ट वे बना रही हैं । उसे बनाने के लिए कच्चा माल कहां से आता है? क्या यह जीवाश्म ईंधन से बने हुए हैं । खुशी की बात यह है कि सभी कंपनियाँ कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए एक लक्ष्य निश्चित किया हुआ है, उसी दिशा में सभी कंपनियाँ काम कर रही हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए सिर्फ कानून बना देने से ही पर्यावरण संरक्षित नही हो जाएगा। उसके लिए हर देश के नागरिक और हर कंपनियों को खुद सोचना पड़ेगा । उस दिशा में खुद काम करना पड़ेगा । तभी पर्यावरण संरक्षित हो सकेगा । नहीं तो कानून तो बहुत पहले से बना हुआ है, इसके बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा में सतत वृद्धि हो रही है ।
अपने इसी उत्तरदायित्व को समझते हुए कंपनियाँ 'कम कार्बन वाली' चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपना रही हैं। कोरेना महामारी के बाद हम सभी को इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या उद्योगपतियों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की ज़िम्मेदारी है। उसे अपने व्यवहार में वह परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था । सरकार, इंडस्ट्री, पैकजिंग इंडस्ट्री, रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री, असरकारी संस्थाएं और देश का हर नागरिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। इसमें नागरिक या उपभोक्ता की भूमिका भी बहुत अहम है। उन्हें प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के निस्तारण व प्रबंधन की दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। इसकी शुरुआत वे अपने घर से कर सकते हैं। उपभोक्ता गीले कचरे को अलग रखें और सूखे कचरे को अलग । इससे कचरे को बेहतर तरीके से निस्तारण करने में मदद मिलेगी। पैकजिंग इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वे इको फ्रेंडली पैकेट्स या कार्टन्स बनाए, जिससे आसानी से रिसायकिल किया जा सके ।
हमारे देश में हर साल 63 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट कचरा इकट्ठा होता है। अगर इसे रिसायकिल करके निस्तारण न किया जाएगा, तो एक दिन हर शहर में कचरे के बड़े-बड़े टीले दिखाई पड़ने लगेंगे ।
हमारी ज़िम्मेदारी जैविक या रीसाइकिलेबल सामग्री को लैंडफिल साइट तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि घर पर ही इसका समाधान वेस्ट सेग्रीगेशन के जरिए किया जाना चाहिए, जिससे वह खाद में बदल जाए या रीसाइकिल हो जाए। इतने बड़े देश में यह करना आसान नहीं है, पर इस दिशा में प्रयास करना जरूरी है। ऐसे में सरकरों और प्रशासन की भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है । पर्यावरण संरक्षण के मामले में पूरे देश के लिए एक कानून बनाना होगा। इससे राज्यों के बीच मतभेद और मनभेद जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी । क़ानूनों में समरूपता न होने की वजह से कंपनियों के लिए नियम को समझना और उसका पालन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाना बहुत जरूरी है। इससे एक बात तो तय हो गई कि पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। और सभी को मिल कर उसे निभाना चाहिए।
प्रोफेसर डॉ. योगेन्द्र यादव
पर्यावरणविद, शिक्षाविद, भाषाविद,विश्लेषक, गांधीवादी /समाजवादी चिंतक, पत्रकार, नेचरोपैथ व ऐक्टविस्ट