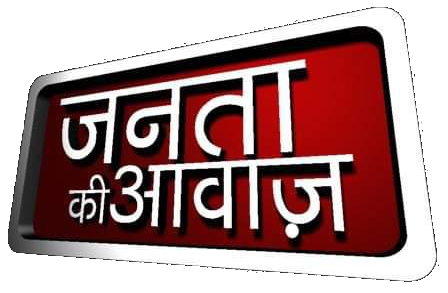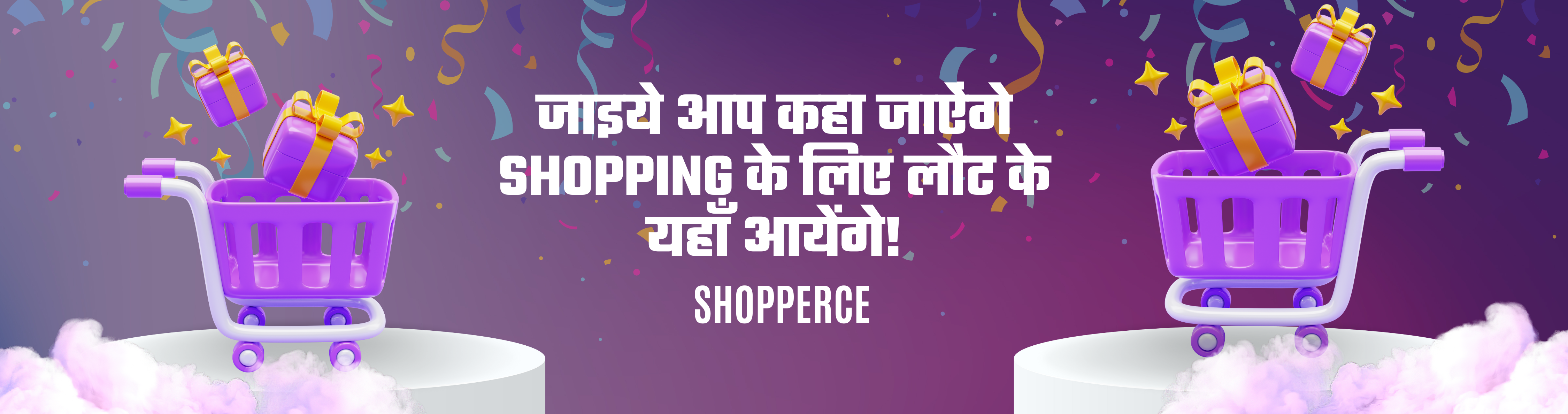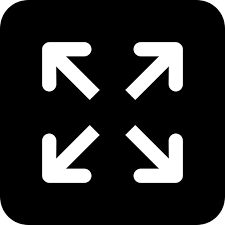सलवा जुडूम की ज्यादतियां और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

(आलेख : संजय पराते)
इंडिया समूह की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी भाजपा के निशाने पर है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के लिए वे जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित सलवा जुडूम पर रोक लगाई थी। इस हिंसक आंदोलन में जो अमानवीय ज्यादतियां हुई थी, उसमें 650 गांवों को जबरन खाली करवाया गया था और इस मुहिम में दर्जनों गांवों को जलाया गया था, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और सैकड़ों की हत्याएं। एक लाख से ज्यादा लोग अपने घरों और गांवों से विस्थापित हुए थे और आज भी हजारों लोग लापता है। नक्सलियों के नाम पर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों द्वारा ग्रामीणों का बड़े पैमाने पर जन संहार किया गया था, जिसकी पुष्टि सीबीआई, मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी विभिन्न जांच रिपोर्टों में की थी, लेकिन आज तक इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया। आदिवासी बच्चों और पूर्व नक्सली तत्वों को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बनाया गया था और इस प्रकार आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ ही खड़ा किया गया था। और यह सब किया गया था बस्तर की प्राकृतिक संपदा की कॉर्पोरेट लूट को आसान बनाने के लिए। सलवा जुडूम पर रोक के बाद भी लूट की यह मुहिम बदस्तूर जारी है और आदिवासियों के उत्पीड़न और उनके मानवाधिकारों के हनन में कोई कमी नहीं आई है। इसके नतीजे में, वर्ष 2011 की जनगणना में बस्तर में आदिवासियों की आबादी में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
जस्टिस सुदर्शन ने अपने एक बयान में स्पष्ट किया है कि सलवा जुडूम पर दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, न कि उनका व्यक्तिगत। उन पर भाजपा द्वारा किए जा रहे हमले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम पर दिए गए फैसले को सार संक्षेप में याद करना उपयोगी होगा, क्योंकि जिस पार्टी का संविधान और संवैधानिक फैसलों पर कोई विश्वास नहीं है, वह न लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है और न मानवाधिकारों का सम्मान। भाजपा आज केवल कॉरपोरेट पूंजी के हाथ का हथियार बनकर रह गई है।
सुप्रीम कोर्ट की इस विवेचना ने राज्य की भाजपा सरकार की उन जनविरोधी नीतियों को बेनकाब कर दिया था, जो नक्सलवाद के दमन के नाम पर आमतौर पर आदिवासियों के दमन, उनके मानवाधिकारों के हनन तथा बस्तर की भूगर्भीय संपदा की लूट के लिए अपनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा प्रहार सरकार की नवउदारवादी तथा वैश्वीकरण जनित नीतियों पर था, जिसकी ‘‘लागत’’ तो गरीबों से वसूली जा रही है, लेकिन ‘‘इसके फायदों के बड़े हिस्से पर समाज के प्रभुत्वशाली तबके का कब्जा’’ हो रहा है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने योजना आयोग द्वारा गठित विषेशज्ञों के समूह की ‘उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौतियां’ नामक रिपोर्ट को उद्धृत किया है -- ‘‘इस कारण इन्हें (आदिवासियों को) अनिवार्य रुप से विस्थापन का सामना करना पड़ा है ... इसने उनके सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों को नष्ट किया है।.... इन सबका मकसद इनके संसाधनों पर कब्जा करना और वंचित लोगों की गरिमा का हनन करना है।’’ (पैरा-6). प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी के हवाले से विकास के इस प्रतिमान को ‘विकास आतंकवाद’ करार देते हुए कोर्ट ने उद्धृत किया है -- ‘‘इसमें राज्य के विकास के नाम पर गरीबों के खिलाफ लगातार हिंसा की जा रही है। राज्य मुख्य रुप से कार्पोरेट अभिजात तंत्र के हित में काम कर रहा है। इस काम में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के साथ ही साथ स्वार्थी राजनैतिक वर्ग का समर्थन भी मिला हुआ है। राजनीतिक समूहों द्वारा इस विकास आतंकवाद को ही प्रगति बताया जा रहा है। .... ‘विकास आतंकवाद’ का सामना करने वाले गरीब अपने सीधे प्रतिरोध से इसे नकार देंगे।’’ (पैरा- 14).
देश के कथित विकास के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के प्रभुत्वशाली वर्ग के पक्ष में दोहन तथा ऊंची विकास दर सुनिश्चित करने के लिए जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, उससे वंचितों और उपेक्षितों तथा मानवीय गरिमा से च्युत लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जिस ऊंची आर्थिक संवृद्धि तथा विकास दर की बात की जा रही है, उसने केवल और केवल, आय के असमान वितरण को ही सुनिश्चित किया है। पूरे देश में चल रही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और इसके खिलाफ जनांदोलनों के उभार से भी यही बात स्पष्ट होती है। कोर्ट ने यह माना है कि 1950-1990 के दौरान 213 लाख लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होना पड़ा है, जिसमें केवल आदिवासियों की संख्या ही 40 प्रतिशत (85 लाख) थी, लेकिन इनमें से केवल 25 प्रतिशत लोगों का ही पुनर्वास किया गया। लेकिन यह फंड-बैंक समर्थित नई आर्थिक नीतियों के लागू किये जाने से पहले के आंकड़े हैं। 1990 के बाद उदारीकरण व वैश्वीकरण की जिन नीतियों को लागू किया जा रहा है, उसके चलते वर्तमान में संख्या अवश्य ही दुगुनी से अधिक हो चुकी होगी। यही ‘वैश्वीकरण का काला पक्ष’ है, जो संपन्न तबकों के चंद लोगों के लिए अधिकांश वंचितों -- और इनमें से लगभग सभी आदिवासी, दलितों तथा आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोग ही हैं -- की बलि मांगता है। इसीलिए कोर्ट की टिप्पणी है कि भारतीय राज्य ने ‘‘जिस झूठे विकास प्रतिमान को बढ़ावा दिया है, उसका कोई मानवीय चेहरा नहीं है।’’ (पैरा- 14). ‘‘राज्य ने सीधे तौर पर संवैधानिक मानकों और मूल्यों का उल्लंघन करके पूंजीवाद के लुटेरे रुपों को समर्थन और बढ़ावा दिया है।’’ (पैरा- 12).
यही वह राजनैतिक-आर्थिक पृष्ठभूमि है, जिससे छत्तीसगढ़ अलग नहीं है। यहां इस देश के कुल लौह अयस्क का 23 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है और हमने देखा है कि किस प्रकार आदिवासियों पर बंदूक तानकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को टाटा के पक्ष में पूरा किया गया था। आज भी किस प्रकार पावर प्लांटों के नाम पर जबरन हथियाये जा रही भूमि के खिलाफ आंदोलनों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। खनिज संपदा की लूट के लिए कुख्यात जिंदल किस प्रकार छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भाजपाई सरकारों की आंख का तारा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है -- ‘‘निश्चित तौर पर ये नीतियां उन सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, जिन्हें ‘गवर्नेंस की बुनियाद’ माना जाता है।’’ (पैरा- 13).
इसीलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित सलवा जुडूम के संदर्भ में यह सवाल प्रासंगिक था कि क्या भाजपा सरकार शासन के लिए संविधान द्वारा निर्देशित मूल्यों और उसकी सीमाओं का पालन कर रही है? (पैरा-16). सुप्रीम कोर्ट का मानना मानना था -- ‘नहीं’, क्योंकि उसकी नीतियां और कारगुजारियां संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (मानव जीवन की गरिमा) का उल्लंघन करती है और यह उल्लंघन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए माओवादियों/नक्सलियों तथा राज्य सरकार और उसकी मशीनरी दोनों को जिम्मेदार माना है। (पैरा- 5). लेकिन कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस दावे को स्पष्ट रुप से ठुकरा दिया है कि नक्सलियों के दमन के नाम पर ‘‘उसे संविधान से यह अधिकार मिला हुआ है कि वह लगातार तथा अंतहीन रुप से मानवाधिकारों का गहरा उल्लंघन करे।... वह चाहे तो इसके लिए माओवादी/नक्सलवादी चरमपंथियों के तरीकों को भी अपना सकता है।’’ (पैरा- 6). उसने छत्तीसगढ़ सरकार की इस मांग को भी ठुकरा दिया था कि संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वह दमन के सहारे शासन करे और इसके लिए बेरहम हिंसा की नीतियों को लागू करने के लिए उसे संवैधानिक मान्यता दी जाये। इसीलिए कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य के बहुत से इलाकों में मौजूद अमानवीय स्थिति तथा मानवाधिकारों के बारे में सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को संदिग्ध और माओवादी या माओवादियों के हमदर्द के रुप में देखे जाने के भाजपाई सरकार के नजरिये को भी खारिज किया है। (पैरा- 4).
अपने आदेश (पैरा- 75) में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम संचालित करने वाले कथित कोया कमांडो या विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए इसे निष्प्रभावी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट केवल निर्दोष आदिवासियों के मानवाधिकारों के लिए ही चिंतित नहीं है, बल्कि वह इन एसपीओ के मानवाधिकारों की ओर भी ध्यान आकर्शित कर रहा है, जिनके ‘‘हाथों में किताबें देने की बजाय बंदूकें थमा दी गई हैं और इन्हें जंगलों की लूट-खसोट में पहरेदार के रुप में खड़े रहने का काम दे दिया गया है।’’ (पैरा- 18). छत्तीसगढ़ सरकार ने एसपीओ को ‘नियमित सुरक्षा बलों का भाग’ माना है, जबकि उनकी नियुक्ति अस्थायी होती थी और उन्हें बहुत ही कम मानदेय दिया जाता था। यह स्पष्ट रुप से उनके मानवाधिकार का हनन था। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अपने हलफनामा में ये झूठा दावा किया था कि ये एसपीओ पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित हैं और माओवादियों से सीधी लड़ाई में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। कोर्ट ने पाया कि अन्य कार्यों के अलावा इन एसपीओ का ‘‘एक मुख्य काम माओवादियों और उनसे हमदर्दी रखने वालों की पहचान करना’’ है। यह कार्य उन्हें सीधे माओवादियों के निशाने पर ले आता था तथा इनका कार्यकाल खत्म होने और सरकार को हथियार वापस करने के बाद ये पूरी तरह असुरक्षित हो जायेंगे। छत्तीगसढ़ सरकार के दावों को ठुकराते हुए कोर्ट ने ये रेखांकित किया है कि 2004-11 के मध्य 6500 एसपीओ में से 291 एसपीओ हताहत हुये हैं, जो कुल एसपीओ का लगभग 5 प्रतिशत हैं, जबकि इसी दौरान नियमित सुरक्षा बलों के केवल 1 प्रतिशत जवान ही मारे गये हैं। सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत शिविरों में हुए नक्सली हमलों में भी बड़ी संख्या में ये एसपीओ ही हताहत हुये हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि एसपीओ के रुप में इनकी नियुक्ति असंवैधानिक क्यों थी? कोर्ट ने कहा है कि ये एसपीओ इतने कम पढ़े-लिखे हैं कि वे आत्मरक्षा की आधुनिक अवधारणा को भी नहीं समझ सकते, ऐसे में उनके द्वारा इन हथियारों का इस्तेमाल गलत तरीके से ही होने की संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि एसपीओ के रुप में भर्ती अधिकांश युवा या तो नक्सली प्रताड़ना का शिकार हैं या फिर भूतपूर्व नक्सली हैं। अतः गुस्से व बदले की भावना के साथ इनका पहले ही अमानवीकरण हो चुका है। लेकिन सरकारी बल में गुस्से व बदले की भावना की कोई जगह नहीं हो सकती। मानसिक अवस्था सही न होने पर ये एसपीओ स्थानीय दुश्मनी भंजाने के लिए किसी को भी माओवादी घोषित कर इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की यह आशंकायें सही थीं। ‘‘मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि एसपीओ और सुरक्षा बलों के द्वारा कई दफा लूट, आगजनी और हिंसा की घटनायें अंजाम दी गई हैं।’’ (पैरा-59). इन एसपीओ ने सलवा जुडूम विरोधी कार्यकर्ताओं पर भी बड़े पैमाने पर हमले किये थे। सलवा जुडूम संचालित क्षेत्रों में एक नागरिक के रुप में भी स्वतंत्र आवाजाही बाधित थी। गांवों पर उन्होंने बड़े पैमाने पर हमले किये थे और जिसमें मोरपल्ली, ताड़मेटला और तिमापुरम गांवों के सैंकड़ों घरों को जलाने, हत्यायें व बलात्कार करने के आरोप लगे थे। इन घटनाओं के उजागर होने के बाद शासन के निर्देश पर तत्कालीन कलेक्टर ने इन पीड़ित गांवों में जो राहत सामग्री भेजने की कोशिश की थी, उसे भी इन एसपीओ द्वारा रोक दिया गया था। स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में जिन लोगों ने प्रभावित गांवों का दौरा करने तथा राहत पहुंचाने की कोशिश की थी, उन पर भी हमले किये गये थे। इस प्रकार इन एसपीओ ने अपनी समान्तर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि लगभग 1200 एसपीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उन्हें बर्खास्त किया गया था। कुल एसपीओ के रुप में भर्ती किये गये लोगों में यह संख्या 20 से 40 प्रतिशत तक बनती थी। किसी भी सरकारी बल में इतनी ज्यादा अनुशासनहीनता का उदाहरण कहीं देखने में नहीं मिलता। लेकिन आपराधिक कार्यवाहियों में लिप्त किसी भी एसपीओ के खिलाफ आज तक सरकार ने कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की है। एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई हैं। जांच के नाम पर केवल लीपापोती की गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था -- ‘‘.... इस तरह के जांच आयोग कानून की जरूरत पूरी नहीं करते : अर्थात् नागरिकों के खिलाफ हुये अपराधों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने जुर्म किया है, उन्हें कानून के द्वारा सजा मिलनी चाहिए।’’ इसी संदर्भ में स्वामी अग्निवेश द्वारा लगाये आरोपों के संदर्भ में कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दिये थे।
एसपीओ के सामर्थ्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी के बाद राज्य की भाजपा सरकार द्वारा उन्हें नियमित सुरक्षा बल के रुप में भर्ती करने के फैसले पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो लोग एसपीओ के लायक नहीं हैं, उन्हें किस प्रकार नियमित सुरक्षा बलों के योग्य माना गया, वह भी योग्यता के मानदंडों में छूट देकर। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार ने सही सबक लेने के बजाय मंत्रिमंडलीय निर्णय और अध्यादेश के जरिये इस फैसले को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई।
81 पैराग्राफों में फैले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की उस समय भी भाजपा ने आलोचना की थी। तर्क यह था कि यह फैसला कार्यपालिका के क्षेत्र में यह न्यायपालिका का अतिक्रमण है। शायद ऐसी आलोचना से सुप्रीम कोर्ट पहले ही सचेत था। अतः उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था -- ‘‘जब न्यायपालिका आतंकवाद और चरमपंथ का मुकाबला करने वाली नीतियों पर सवाल उठाती है, तो उसका मकसद यह नहीं होता है कि वह सुरक्षा चिंताओं में दखल दे। हम ये मानते हैं कि इसके लिए कार्यपालिका के पास विषेशज्ञता और जिम्मेदारी है, और कार्यपालिका, विधायिका से निर्देषित और नियंत्रित होती है। न्यायपालिका इस तरह के मसलों में संवैधानिक लक्षणों और मूल्यों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है। वह चाहती है कि समानता और जीवन के अधिकार जैसे मूल अधिकारों की सुरक्षा हो। सच्चाई यह है कि न्यायपालिका के पास इस तरह हस्तक्षेप करने की विषेशज्ञता और जिम्मेदारी है।’’ (पैरा-68).
सलवा जुडूम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भाजपा नेता अरुण जेटली ने इसे ‘विचारधारा आधारित निर्णय’ करार दिया था। आज गृह मंत्री अमित शाह भी हमला कर रहे हैं। आज जब भारतीय संविधान में निहित उद्देश्यों पर चलने की बात न्यायपालिका करती है, तो उसे खारिज करने की कोशिश की जाती है। नक्सलवाद को ‘कानून व्यवस्था’ की समस्या मानते हुए दमन के बल पर इसका हल खोजने की कोशिश की जाती है, जबकि स्पष्टतः ‘‘मूल समस्या की जड़ राज्य द्वारा अपनाई गई सामाजिक-आर्थिक नीतियों में निहित’’ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकारों को उस संवैधानिक दर्शन के धरातल पर परखने की कोशिश करता है, जो ‘‘...गरीबों में असंतोष उत्पन्न करने वाली सामाजिक-आर्थिक नीतियों को अपनाने के विचार को पूरी तरह नकार देता है।’’ (पैरा-20). लेकिन इसके बावजूद जो एक ओर तो निजी क्षेत्र को टैक्स छूट के रुप में लगातार सब्सिडी दे रहा है, तो दूसरी ओर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा गरीबों की मदद करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होने का रोना रोता है। (पैरा-15).
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट रुप से यह कहता है कि राज्य और देश के नागरिकों के जान-माल की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि संविधानेत्तर किसी सत्ता की। इस प्राथमिक जिम्मेदारी से कोई भी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। इस फैसले की आलोचना करने वाली वाली भाजपा वैचारिक-नीतिगत स्तर पर किस धरातल पर खड़ी है, यह साफ है। उन्हें लुटेरे पूंजीवाद के साथ खड़े होने के साथ कोई हिचक नहीं है, संविधान जाये भाड़ में! गनीमत यही है कि अमित शाह ने जस्टिस सुदर्शन पर माओवादी होने का आरोप नहीं मढ़ा है!!
सलवा जुडूम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संवैधानिक निर्णय था, लेकिन भाजपा का इस देश के संविधान और उसके मूल्यों, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों और मानवाधिकारों पर कोई विश्वास नहीं है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर हमला इसी तथ्य को साबित करता है।