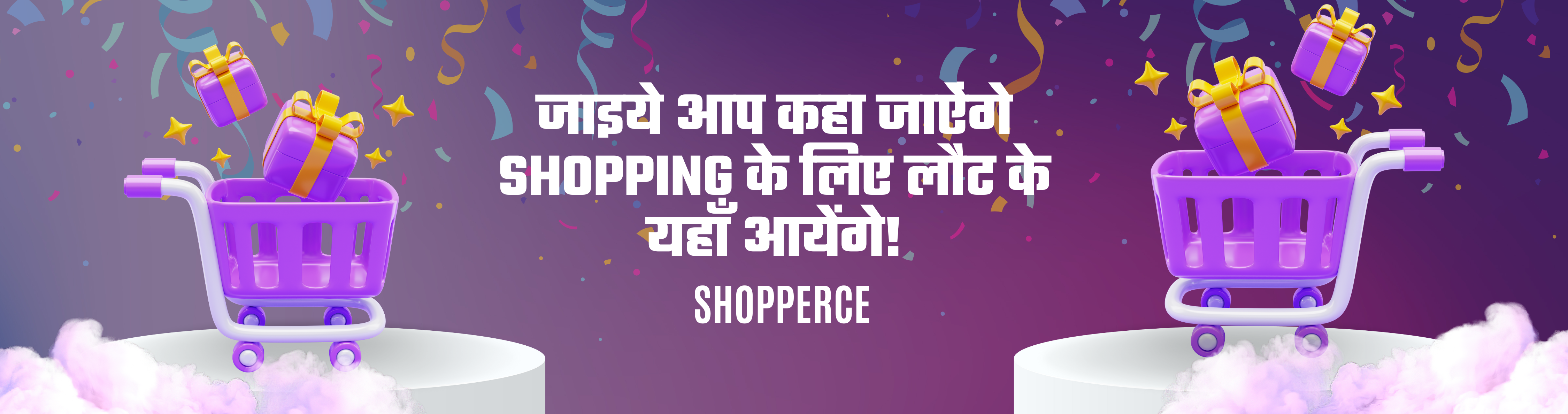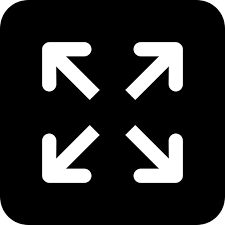क्या भारत का लोकतंत्र अब ‘नियंत्रित लोकतंत्र’ में बदल गया है?

(आलेख : कृष्ण प्रताप सिंह)
अंदेशे तो पहले से जताए जा रहे थे, लेकिन अब देश के चुनाव आयोग ने जिस तरह सारी लोकलाज (जिसे लोकतांत्रिक बर्ताव का सबसे जरूरी तत्व बताया जाता है) बिसराकर अपनी (अ)विश्वसनीयता से जुड़े सारे सवालों की जवाबदेही की ओर पीठ कर ली, साथ ही चोर के कोतवाल को डांटने की तर्ज पर विपक्षी दलों व नेताओं के विरुद्ध हमलावर रवैया अख्तियार कर लिया है, उससे एक तरह से पुष्टि हो गई है कि हम नियंत्रित, प्रबंधित या निर्देशित लोकतंत्र में रहने को अभिशप्त हो गए हैं।
वैसे इस बाबत यह कहना ज्यादा सही होगा कि देखते-देखते देश के संवैधानिक लोकतंत्र को नियंत्रित लोकतंत्र (कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी) में बदल डाला गया है। लगातार कटौतियों की मार्फत उसे आंशिक कर देने की लगातार चल रही कोशिशें तो खैर अब दस-ग्यारह साल पुरानी हो चली है।
राजनीति-विज्ञानियों के अनुसार, नियंत्रित लोकतंत्रों में सरकारें ऊपर-ऊपर से अपने लोकतांत्रिक होने का दिखावा भले करती रहती हैं, अपनी वास्तविक शक्ति कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में केंद्रित कर देती हैं। ऐसे लोकतंत्रों में चुनाव पहले से तय किए गए परिणामों को वैध करार देने भर के लिए कराए जाते हैं और उनके पीछे सरकारी नीतियों को बदलने की मतदाताओं की शक्ति को निरुपाय कर देने की बदनीयती होती है।
जाहिर है कि ऐसे में मतदाताओं का पोलिंग बूथों तक जाना औपचारिकता भर रह जाता है और चुनावों की स्वतंत्रता व निष्पक्षता कोई बड़ा मूल्य नहीं रह जाती। चूंकि इस सबके लिए स्वतंत्र मीडिया को सत्ता समर्थक मीडिया में बदलना जरूरी होता है, इसलिए उस पर भी तरह-तरह के शिकंजे कसकर उसे सिर उठाने लायक नहीं रहने दिया जाता।
स्वाभाविक ही, नागरिकों के अधिकार सरकारों की सहमति के मोहताज हो जाते हैं और चूंकि सरकारों की वास्तविक शक्ति कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में केंद्रित होती है, इसलिए वह नागरिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील या जवाबदेह होने की जरूरत महसूस नहीं करती। तब सत्तासेवी व्यक्तियों या समूहों को चुनावों को प्रायोजित और जनसंचार माध्यमों या मीडिया का लोगों के ब्रेनवॉश के लिए इस्तेमाल करने की ‘आज़ादी’ मिल जाती है।
कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे लोकतंत्रों में जनता के अपने प्रतिनिधि या शासक चुनने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के अधिकार का कोई खास मतलब नहीं रह जाता।
नियंत्रित न होता तो
अपने देश के संदर्भ में बात को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र नियंत्रित नहीं हो गया होता और चुनाव आयोग की शक्तियां उसी में निहित होतीं, तो अव्वल तो वह ऐसी स्थिति बनने ही नहीं देता, जिसमें वोटों की ऐसी गुपचुप चोरी हो और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उसका खुलासा करना पड़े।
दूसरे, किसी कारण ऐसी स्थिति बन भी जाती, तो आयोग फौरन उसको बदलने में लग जाता, ताकि चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को लेकर आम लोगों के मनों में पनप गया अविश्वास घटे, न कि और गहराए।
तब वह राहुल गांधी द्वारा उल्लिखित वोट चोरी के पांचों तरीकों की बाबत तथ्यात्मक व भरोसेमंद सफाई पेश करता और उनके सिलसिले में उठाए जा रहे सारे सवालों के समुचित जवाब देता। सफाई संभव न होती, तो वह आगे ऐसी चोरी न होने देने के पक्के इंतजाम सुनिश्चित करता।
साथ ही समझता कि कोई भी संवैधानिक संस्था, वह चाहे कितनी भी ऊंची व ताकतवर हो, अंततः जनता के प्रति ही उत्तरदायी है और उसी जनता ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाकर उसे प्रश्नांकित करने व कठघरे में खड़ा करने का अधिकार दिया है।
इसके विपरीत वह जिस तरह उल्टे समूचे विपक्ष पर हमलावर होकर सत्तादल के नैरेटिव को आगे बढ़ाने में अपने अंतिम लज्जावसन तक उतारने और अपने दामन में लगी कालिख को और गहरी करने की कवायदों में मुब्तिला है, बावजूद इसके कि सर्वोच्च न्यायालय भी उससे खुश नहीं दिखता, उससे शायद ही इस बाबत किसी को संदेह हो कि इस ‘लोकतंत्र’ में उसका नियंत्रण कहां से होने लगा है।
हद तो यह कि उसे और उसके ‘नियंत्रक’ को ठीक से यह समझना भी गवारा नहीं है कि अगर चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष न रह जाएं, तो वे लोकतंत्र की प्राणवायु नहीं रह जाते और चुनाव करा देने भर से कोई देश या उसकी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो जाती।
चुनाव होना भर लोकतंत्र नहीं
मिसाल के तौर पर रूस में भी चुनाव आयोग है और वहां भी संसद व राष्ट्रपति के नियमित चुनाव होते हैं। विभिन्न दलों के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरते ही हैं। लेकिन यह सब किसी ढकोसले से ज्यादा नहीं होता। इसीलिए गत ढाई दशकों से व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन व उनकी पार्टी ही सत्ता पर काबिज है।
इतना ही नहीं, उनकी सरकार का विरोध करने व सच्चाई उजागर करने वालों का स्थान देश की जेलों में है।
ऐसे में कोई सच्चा लोकतंत्र प्रेमी रूस को लोकतांत्रिक देश क्यों कर कहेगा?
प्रसंगवश, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी चुनाव के जरिए ही सत्ता में आया था और चुनाव जीतकर ही सत्ता पर काबिज भी रहा। पर केवल चुनाव करा देने भर से कोई उसको, उसके शासनकाल या देश (जर्मनी) को लोकतांत्रिक नहीं कहता।
सच्चे लोकतंत्र में चुनावों के यथासमय होने से कहीं ज्यादा जरूरी उनका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना होता है, जो तभी संभव है, जब चुनाव कराने वाली मशीनरी पूरी तरह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से काम करे। यह तभी संभव है, जब चुनाव आयोग इसके प्रति दृढ़ संकल्पित हो।
उसका यह दृढ़ संकल्प सुनिश्चित करने के लिए ही हमारे संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को यह सुरक्षा दी गई है कि एक बार नियुक्ति के बाद उन्हें संसद के दोनों सदनों में पारित महाभियोग प्रस्ताव के जरिए ही हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव का संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना भी अनिवार्य किया गया है।
इसके बावजूद, चूंकि देश में नियंत्रित लोकतंत्र की स्थिति बना दी गई है, वास्तविक लोकतंत्र में चुनाव आयोग से की जाने वाली यह अपेक्षा पूरी नहीं हो रही कि वह न केवल स्वतंत्र, बल्कि निष्पक्ष भी रहे। दुर्भाग्य यह कि आयोग अपनी निष्पक्षता महज मुख्य चुनाव आयुक्त के इस जबानी जमा-खर्च से साबित करना चाहता है कि उसकी निगाह में विपक्ष व सत्तापक्ष सब समकक्ष हैं। काश, इस समकक्षता को वह अपने आचरण में भी उतारना चाहता!
दूसरी ओर बिहार में उसकी कारस्तानियों पर संसद में चर्चा की विपक्ष की मांग के सिलसिले में न उसकी समर्थक सरकार, न ही सत्तारूढ़ दल यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था संसद के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद ही सर्वोच्च संस्था तथा जनता की इच्छा का दर्पण है।
उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है कि यदि संसद को मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाने का अधिकार है, तो वह उनके आचरण पर बहस क्यों नहीं कर सकती? खासकर जब वे प्रेस कांफ्रेंस तक में निर्लज्जतापूर्वक भाजपा और उसकी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, जो निश्चय ही लोकतंत्र के लिए गहरा सदमा है। ऐसा सदमा, जो उसने लोकतंत्र के स्रोत को ही विषाक्त करके पैदा किया है।
पूरे कुएं में भांग
लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग की ही बात क्यों की जाए? हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के नियंत्रित लोकतंत्र में बदल जाने के कारण संसद व राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाएं हों या सीबीआई व ईडी जैसी वैधानिक संस्थाएं, कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर पा रहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बार-बार प्रश्नांकित होने से नहीं बच पा रही।
प्रचारित भले किया जाता है कि संवैधानिक व वैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र ढंग से काम करती व निर्णय लेती हैं, व्यवहार में वे इसके उलट सत्ता, खासकर उसके प्रमुख के इशारे पर काम करने लगी हैं। वे उसी की भाषा बोलती हैं और उसके कृत्यों में कितना भी खोट क्यों न हो, उन पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाती।
अब तो हम यह भी देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तक सत्ता के इशारे पर काम करते हैं और नहीं करते, तो जगदीप धनखड़ की गति को प्राप्त हो जाते हैं।
फिर आईएएस या आईपीएस अफसरों यानी नौकरशाहों की बात भी क्या की जाए! विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, विभिन्न प्रकार के आयोगों के अध्यक्षों, उच्च तकनीकी व मेडिकल संस्थाओं के प्रमुखों का हाल भी कुछ अलग नहीं है और वे भी ‘ऊपर के इशारे पर’ ही काम करने लगे हैं। इसके चलते, न उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णय स्वतंत्र व निष्पक्ष रह जाते हैं, न ही नियुक्तियां, न ही उनके उठाये अन्य कदम।
अब यह तो कोई बताने की बात भी नहीं है कि इस नियंत्रित लोकतंत्र में चारों ओर सत्ताधीश के जयकारे का शोर है, जो इसलिए मचाया जा रहा है, ताकि उसकी आड़ में सारी विद्रूपताओं को गुरूर के साथ सफलतापूर्वक नेपथ्य में डाला जा सके।
('द वायर' से साभार। लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)