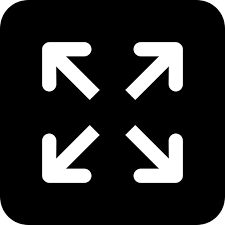'परत' में गाँव है..मेरे गाँव की तरह....
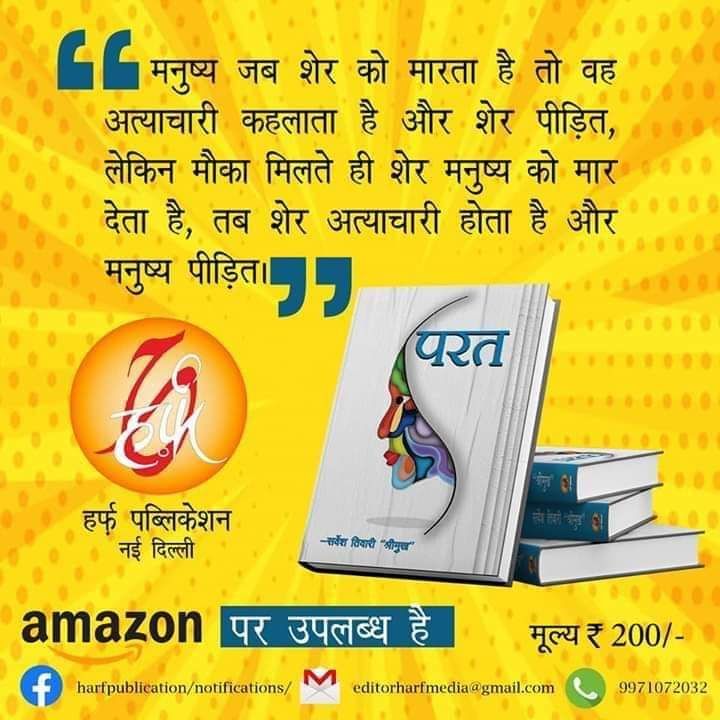
करीब बारह साल हुए..मैं बीए द्वितीय वर्ष में था..सत्रह अठारह साल की उम्र बड़ी जोरदार होती है..रचनात्मकता और कलात्मक सृजन का बोध अपने शीर्ष पर होता है। मेरे पास भी एक कवि हृदय था..एक डायरी थी, जिसपर मैं कविताएँ लिखा करता था।
कविताएँ लिख तो लेता था, लेक़िन उन कविताओं को समझने वाले और सराहने वालो का इतना टोटा था कि उन्हें डायरी से बाहर आने में बड़ा समय लगा। वो दौर ऐसा था जहाँ हिंदी में लेखन हँस, क़ादम्बिनी या ऐसी ही प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने से आदर पाता था। अखबारों के संपादकीय में छपे लेखों के नीचे काले मोटे अक्षरों में लिखे लेखक के नाम को पढ़कर मेरे जैसा तथाकथित कवि हृदय व्यक्तित्व बस आहें भरकर रह जाता था और सोंचता रहता था कि ये जिनके नाम छप रहे हैं, वो जरूर मेरी तरह के नहीं होंगे..उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन सबकुछ एक फैंटेसी की तरह मेरी कल्पनाओं में घूमता रहता था।
ऐसी ही ठंढ़ के दिन थे..मैं अखबार पढ़ रहा था..पढ़ते पढ़ते कुछ मन हुआ और उस अखबार पर ही चार पंक्तियाँ लिख गया..
"कल स्वप्न तुम्हारे देखे थे मैंने रजनी के आँचल में,
एक स्याह उमड़ सी आई थी तुम्हारे नैनों के काज़ल में..
जो वक्त ठहर जाता तो कुछ बाते हम कह जाते,
पर शब्द मेरे पुलकित हो भागे कुछ कोहरे कुछ बादल में.."
आज इस कविता को देखता हूँ तो अपनी उस उम्र को शाबासी देने का मन होता है क्योंकि ठीकठाक भाव हैं इन चार पंक्तियों में। लेक़िन, इस कविता के पहले पाठक जो मेरे रिश्ते के एक चाचा ही थे, की प्रतिक्रिया थी..
"अच्छा! त एह घरी शेर लिखा ता, गदहा कहीं का!.."
ये 'गदहा कहीं का' उस दौर के मेरे जैसों का सत्य था..क्योंकि, हमारी कोई सींघ पूँछ तो थी नहीं जो हमें नोटिस किया जाता..और लोवर मिडिल क्लास के लड़कों के लिए टैलेंट का एकमात्र मतलब सरकारी नौकरी पहले भी रही है, तब भी थी और आज भी है।
फ़िर समय ने एक करवट बदली और दौर आया सोशल मीडिया का...एक ऐसा मंच जहाँ अपनी बात कहने के लिए कोई संकोच नहीं था। बिना ये देखे कि मेरे बारे में मेरे बगल के घर मे क्या बात होगी, किसी अनदेखे घर में स्वयं की बात पहुंचाने का एक माध्यम मिलता सा लगा।
सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में भी कहानी बहुत नहीं बदली..बस इतना हुआ कि जिन्हें हम अखबारों में देखते थे उन्हें अब इंटरनेट पर देखने लगे अपनी आत्ममुग्धता का प्रचार करते।
फिर थोड़ा समय बीता और स्मार्टफोन्स के साथ सोशल मीडिया भी हर हाथ पहुंचता गया और ये पहुँच तब के मेरे जैसों को यहाँ ले आई जहाँ डायरी किसी के देख भर लेने से सहम जाने वाली बात नहीं थी बल्कि औरों के अनुभवों से खुद को और बेहतर करने का अवसर था।
इसी फ़ेसबुक पर कहीं एकबार पढ़ा था कि फ़ेसबुक से ही एकदिन सैकड़ों प्रेमचंद निकलेंगे। यहाँ प्रेमचंद का मतलब वो नहीं जो बढियाँ लिखते हैं..बढियाँ तो रवीश कुमार, शिव खेड़ा, ओम थानवी, आशुतोष राणा जैसे बहुत लोग लिखतें हैं..प्रेमचंद का मतलब है वो व्यक्ति लिखे जो प्रेमचंद की तरह ही अपने 'लोक' को जी रहा हो..जो लिख रहा है उसे जी भी रहा हो..जो जी रहा है उससे सीख भी रहा हो..
करीब पाँच साल पहले फ़ेसबुक पर गोपालगंज के एक शिक्षक मित्र से परिचय हुआ जिनकी उनदिनों की फेसबुक पोस्ट्स भी बहुत बढियाँ होती थी..किंतु, ईमानदारी से कहूँ तो उन्हें आधार मानकर ये कहना उनदिनों लगभग असंभव था कि यह व्यक्ति कभी एक पूरी किताब लिख सकता है। और इसीलिए जब ये चर्चा हुई कि Sarvesh भईया कि किताब 'परत' प्रकाशित होने वाली है तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई क्योंकि सर्वेश को भी मैं अपनी वाली 'फ़ेसबुकिया प्रेमचंदों' की बिरादरी का ही मानता हूँ...
ख़ैर, परसो शाम को 'परत' एमेजॉन की कृपा से मेरे हाथों में थी।
बड़े बड़े कहे जाने वाले बहुत से लेखकों की किताबें खरीदता हूँ और फिर दो चार पन्ने पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों अपनेआप किताबें मेरे शीशे वाली आलमारी में चली जाती हैं, समझ में नहीं आता..हो सकता है वो बहुत बड़ी बात लिखते हों जिन्हें मेरी बुद्धि समझ नहीं पाती..
अरे! ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि जब पाठक ही मेरी बुद्धि का है तो फिर कोई बहुत ऊँची बात लिखकर उससे कैसे जुड़ सकता है???? और मुझे ये बात भी इसीलिए समझ में आई क्योंकि बैंक से लौटकर दो घँटे के भीतर मैं आधी किताब पढ़ गया था।
क़िताब शुरू होती है दो सहेलियों श्रद्धा और शिल्पी के साथ जो बिल्कुल वैसे ही गाँव में रहती हैं जहाँ से लगभग हमसब या फ़िर हमारे जैसे हैं। उस गाँव में भी अरविंद सिंह नाम के एक बाहुबली प्रतिनिधि वैसे ही हैं, जैसे हमसबके गाँवो में होते हैं। आलोक पांडेय नाम का एक दूसरा क्षत्रप उस गाँव में भी है जैसा हमसबके गाँव में होता है। आलोक पांडेय और अरविंद सिंह में भी तनाव है, वैसे ही जैसे हमारे गांवों के दो शक्तिशालियों में होता है और हमारे गाँव के लोग कभी उनकी तरफ़दारी में तो कभी उनकी चापलूसी में और कभी उनके प्रभाव से मूर्ख बनकर आपस में कभी न समाप्त होने वाला बैर पाल बैठते हैं, इस बात से बेखबर होकर कि आलोक पांडेय और अरविंद सिंह दोनों ही भारत के लोकतंत्र का सम्भवतः उसी तरह उपहास करते हैं जैसे संसद में एक दूसरे को हमेशा कोसने वाले नेताओं के वेतन और भत्तों की अश्लील वृद्धि को बिना किसी मतभेद के ताली पीटकर ध्वनिमत से पारित करा देते हैं। आलोक और अरविंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी एक नहीं होंगे तो अलग भी नहीं हो सकते।
'परत' की नायिका शिल्पी है जिसके पिता विनोद लाल और माँ गायत्री न जाने क्यों पूरी किताब ख़त्म होने तक मुझे अपने साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाते महसूस हुए। मुझे लगता है जिनकी भी बेटियाँ हैं उन्हें अपनी मनोदशा एकदम विनोद लाल और गायत्री जैसी ही लगेगी।
'परत' में गाँव है..मेरे गाँव की तरह ही हर गाँव की वर्तमान स्थिति की परत दर परत तहे खोलती यह किताब जब मेरे जैसे व्यक्ति को पहले पन्ने से आखिरी तक एकबार में उठने नहीं दी तो ये सत्य है कि इसे पढ़ने वाले लोगों में कमसेकम 80% इसे एकबार में ही पढ़ेंगे।
भाषा शैली कई बार ऐसा लगती है जैसे श्रीलाल शुक्ल और रेणु से प्रभावित हो...लेक़िन, चूँकि मैं सर्वेश भाई को व्यक्तिगत रूप से जनता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आज के दौर के अधिकतर लेखक जहाँ अपनी किताबों से पहले अपनी डिग्रियों की मार्केटिंग करने लगे हैं, भईया इतिहास से एमए पास भर हैं। हिंदी साहित्य वो भी लगभग उतना ही पढ़े हैं जितना कि सम्भवतः मैं स्वयं...कईबार ऐसा लगता है कि कटाक्षों का अतिरेक हो रहा है कहीं कहीं कि तभी कोई ऐसी पंक्ति आ जाती है जिसे बारबार पढ़ने के बाद भी हटने का मन नहीं करता कि कहीं ये बात दिमाग से उतर ना जाए..जैसे...
"मनुष्य के अंदर यदि बड़ा कहलाने की हवस न हो तो वह विपन्नता में भी मुस्कुरा सकता है।"
"व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं की संख्या बताती है कि बाजार ने उसे किस हदतक मूर्ख बनाया है।"
"भागने वाली लड़कियाँ नहीं समझती कि उनके सपनों का मूल्य उनके भाई बहन अपने अश्रुओं से चुकाते हैं।"
"प्रेम और कुछ सिखाए न सिखाए, सबसे पहले झूठ बोलना और छल करना सिखा देता है।"
'परत' में दो कहानियाँ समानांतर रूप से चलती है जिसे पढ़ते पढ़ते एक बार 'मसान' फ़िल्म का ध्यान जरूर आ जाता है..सोनू और शिल्पी का रोमांस यश चोपड़ा की कुछ फिल्मों की याद दिला देता है...लेक़िन, लगभग सभी दृश्यों में भाव कुछ ऐसे उत्पन्न होते हैं कि लेखक सिनेमा से प्रभावित नहीं लगता।
मुझे याद है कि एकबार तब रोया था जब प्रेमचंद की निर्मला आख़िरी कुछ पन्नो में अपनी आख़िरी साँसे ले रही थी। किसी किताब को पढ़कर आँखे भिगोने का यह दूसरा अवसर है जब विनोदलाल की गोद मे सर रखकर गायत्री ने अपनी आँखें मूँद ली। मेरी भीगीं आँखें फूटफूटकर रोने लगी जब गाँव के कुछ लड़के 'खर' ले आते हैं, कोई बाँस की व्यवस्था कर लाता है, कोई दौड़कर लुहार बुला लाता है, कुछ लड़के गायत्री के शव को उतारकर ज़मीन पर सुला देते हैं। विनोदलाल भी तो रोते हैं फूटफूटकर क्योंकि उनके लिए पत्नी नहीं उनका पूरा घर मर गया था। सच में हमारे यहाँ स्त्रियां ही हमारा पूरा घर होती हैं।
मुझे पता है कि अभी ये इस किताब का शुरुआती दौर है। अभी पाठकों पर इसका पहला प्रभाव पड़ा है। समय के साथ इस किताब की भी समीक्षा होगी, नाखूनों से इसकी भी कमियाँ बकोटने का प्रयास भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां नहीं है। कमियाँ तो कालिदास, तुलसी से लेकर जायसी, कबीर प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त में भी खोजी गई हैं। अंग्रेजी साहित्य में भी जॉन लिली, टॉमस किड, क्रिस्टोफ़र मार्लो से लेकर शेक्सपियर, टेनिसन, इलियट और पीबी शैली की भी आलोचना हुई है।
इस किताब की भी आलोचना होगी।
परन्तु, मेरे लिए ये किताब एक उपन्यास से बढ़कर एक प्रेरणा है, जो इसे साहित्यिक गुणदोष के परे जाकर पढ़ने की वकालत करती है। मुझे ये लगता है कि ये किताब उत्तर भारत के हर मिडिल क्लास के घर में होनी चाहिए जिससे हर परिवार अपने बड़े होते बच्चों के साथ इसे पढ़े और सीखे कि वास्तव में प्रेम वो है जो प्रेम हो।
ये किताब आज हर दो घर छोड़कर उत्पन्न हो रही शिल्पियों को रोक सकती है। इस किताब में वो बात है जो विनोदलाल और गायत्रियों को सम्हाल सकती है। ये किताब सिखा सकती है कि हर शिल्पी के भाग्य में श्रद्धा नहीं हो सकती लेकिन, हर विनोदलाल के भाग्य में शिल्पी भी तो नहीं होनी चाहिए।
सर्वेश भाई!
आप बड़े भाई हैं, फ़िरभी सम्मान के साथ आपसे ईर्ष्या हो रही है। अभी मैंने करीब पंद्रह 'परत' ऑर्डर की हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये किताब लिटरेचर के लिए नहीं एक धरोहर के रूप में पढ़ी जानी चाहिए।
सौरभ चतुर्वेदी
बलिया