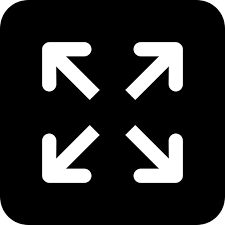''गुलों में रंग भरे बाद-ए-नौबहार चले..चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले'', मशहूर शायर फ़ैज़ की पुण्यतिथी आज

नई दिल्ली । 'जितना मुश्किल है फ़ैज़ दिखना भी, उतना मुश्किल है फ़ैज़ होना भी।' भारतीय उपमहाद्वीप में शायरी का जिक्र हो और उसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जि़क्र न हो, यह मुमकिन नहीं है। यह ठीक है कि ग़ज़ल ने कबीर और अमीर खुसरो से अब तक कई रंग देखे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ग़ज़ल की रूह को समझा और उसे सींचा, उनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम बहुत अदब और एहतराम से लिया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1984 में लाहौर पाकिस्तान में उनका निधन हुआ था।
13 फरवरी 1911 को सियालकोट पाकिस्तान में जन्मे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कुछ समय तक दिल्ली में भी रहे। उन्होंने अमृतसर कॉलेज में भी पढ़ाया और फिर पाकिस्तान चले गए। वह सर गंगा राम वाले लाहौर (पाकिस्तान) के बाद में हुए, सबसे पहले वह दिल्ली और अमृतसर (भारत) के रहे। यहां तक कि रूसी महिला एलिस फ़ैज़ के साथ शादी करने के बाद 1941 में वह कुछ समय दिल्ली में ही रहे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह मुल्कों की सरहद के सच को स्वीकार तो करते थे, लेकिन उनके अपने जेहन की कोई सरहद नहीं थी।
यही कारण है कि वह बेरुत से लेकर फिलीस्तीन तक कुछ अप्रिय देखने पर द्रवित हो जाते थे। भारत अक्सर आते थे और कभी उनकी जुबान से भारत विरोधी शायरी नहीं सुनी गई। हालांकि यह काम भारत के कुछ नामी शायर भारत से बाहर के मुशायरों में अब भी करते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी ग़ज़ल की रूह को चुटकलों ने घेर लिया है और वह नारेबाज़ी को ही शायरी की नई परिभाषा बताने लगे हैं।
इस एतबार से फ़ैज़ को याद करना 'गुलशन के कारोबार' को चलाने की कोशिश करना है। बाद-ए-नौबहार के चलने का मंज़र देखने जैसा है। एक्टिविस्ट, फौजी, प्राध्यापक, संपादक और न जाने कितनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते फ़ैज़, आज भी अपना फ़ैज़ बिखेर रहे हैं। वह विचारधारा से अवश्य वामपंथी रहे, लेकिन उनके व्यक्तित्व, और शायरी का ढांचा कई खूबियों पर खड़ा है।
पहली खूबी है, गम-ए-दौरां को महसूस करना या समाज के दुख को समझना और दूसरी खूबी है गम-ए-जानां यानी महबूब के दुख को समझना। उनके लिए प्रेम भी क्रांति थी और क्रांति भी प्रेम था। यही कारण रहा कि उनकी ग़ज़लें अपने क्लासिकल रचाव में भरपूर रंगी हुई रहीं। ग़ज़ल का सम्मान बरकरार रखने वालों में फ़ैज़ का नाम ऊपर ही रहेगा। उनका बहुत चर्चा में नहीं आ पाया यह शेर कुछ कहता है-
'ग़मे-जहां हो, ग़मे-यार हो कि तीरे-सितम
जो आये, आये कि हम दिल कुशादा रखते हैं'
यह कुशादा यानी खुला हुआ दिल रखने की यह क्षमता ही फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का 'फ़ैज़' यानी प्रकाश बिखेरती है। ज़माने का दुख हो, महबूब का गम हो या कोई भी सितम, फ़ैज़ हमेशा दिल खोल हुए रहे। दरअसल ऐसे लोग, ऐसा माहौल, कुछ नायाब आवाजों का मिश्रण हो जाते हैं। कव्वाली के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में उनकी गाई हुई ग़ज़ल किस जहां में ले जाती है, यह सुनने वाला ही जानता है-
'तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है,
न शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से है'
उनकी शायरी बहुत लोगों ने गाई। पाकिस्तान में भी और भारत में भी। हालांकि जिसकी आवाज़ ने फ़ैज़ साहब को पूरी दुनिया से परिचित करवाया, वह थे मेहदी हसन साहब। राजस्थाान की रेत में तपी हुई आवाज़ जिसमें फ़ैज़ को सुन कर फ़ैज़ अपने हो जाते थे।
'तुम आये हो न शब-ए-इन्तज़ार गुज़री है
तलाश में है सहर बार बार गुज़री है'
या फिर
'गुलों में रंग भरे बाद-ए-नौबहार चले
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले'
इन ग़ज़लों को सुन कर कौन पहले जैसा रह पाता है? आज न नुसरत हैं, न मेहदी हसन और न ही फ़ैज़ लेकिन ये आवाजें हमारे सन्नाटे को चीरने का दम रखती हैं।
यह सवाल अक्सर उठता रहा है कि शायर अपने साथ बीती को लिखे या फिर औरों के दुख को जीकर लिखे? फैज की शायरी इसी सवाल का जवाब देती प्रतीत होती है। गमेजहां का हिसाब करते हुए किसी का स्मरण हो आना या फिर यह कहना कि 'राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा'। यह फैज का ही कमाल था। प्रेम हो या विद्रोह दोनों में संवेदनाओं की जरूरत होती है।
प्रतिबंध के बावजूद इकबाल बानों ने साड़ी पहन पढ़ी थी ये नज्म
उनका लिखा साहित्य खासतौर पर गज़़ल और नज्म के रूप में बाहर आया। परीखाने से लेकर बाजार में बिकते हुए मजदूर के गोश्त तक उनकी नजर इसीलिए जाती है, क्योंकि वह रोजगार के गम तक भी पहुंचते हैं। वह जानते हैं कब शायर को ऐसा कहना चाहिए कि 'मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग।' इकबाल बानो ने उनके बहुचर्चित नज्म 'हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे' के साथ पूरा न्याय किया है। यह एक अलग किस्सा है कि 1985 में जि़या उल हक के सैन्य शासन में जब साड़ी पर पाबंदी थी, इकबाल बानो ने यही नज्म साड़ी पहन कर करीब 50,000 लोगों के सामने गाई थी।
'बड़े शायर न होते तो भी बड़े इंसान ही होते'
'नक्श-ए-फरियादी, 'दस्त-ए-सबा, 'जिंदानामा, 'दस्त-ए-तहे-संग, 'मेरे दिल मेरे मुसाफिर, 'सर-ए-वादी-ए-सिना आदि संग्रहों के रचयिता फ़ैज़ की हिंदी, अरबी, अंग्रेजी उर्दू और रूसी भाषाओं के भी जानकार थे। वह बेशक आज हमारे बीच सशरीर न हों, साहित्य खासतौर पर ग़ज़ल और नज्म से बाबस्तगी रखने वाली नई नस्ल उनसे रोशनी ले रही है। उनके चाहने वालों में से लगभग सभी का मानना है कि वह बड़े शायर न भी होते तो भी अपने खुलेपन और शादगी के कारण एक बड़े इन्सान ही होते।
टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे
मज़े की बात यह है कि वह टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाने का उन्हें अफसोस रहा। एक साक्षात्कातर में उन्होंने नए शायरों को जो संदेश दिया था, वह जस का तस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 'भई ...हम परवरिश-ए-लौह-ओ कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है, रकम करते रहेंगे। यानी....सच लिखो यार, झूठ मत लिखो, यह तो ठीक नहीं, सोच कुछ रहे हो, लिख कुछ रहे हो। ऐसे में कोई कितना भी बड़ा कारीगर क्यों न हो या क्राफ्ट वर्क में माहिर क्योंं न हो जाए, पता चल जाता है कि बात नक्काली में कही है, किसी की खुशामद में कही है, फैशन में कही है, लालच में कही है....।'
फ़ैज़ की एक बेहद मशहूर नज्म
'मुझ से पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न माँग
मैं ने समझा था कि तू है तो दरख़शाँ है हयात
तेरा ग़म है तो ग़म-ए-दहर का झगड़ा क्या है
तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है
तू जो मिल जाये तो तक़दीर निगूँ हो जाये
यूँ न था मैं ने फ़क़त चाहा था यूँ हो जाये
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा
राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा
मुझ से पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न माँग
अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाना तलिस्म
रेशम-ओ-अतलस-ओ-कमख़्वाब में बुनवाये हुये
जा-ब-जा बिकते हुये कूचा-ओ-बाज़ार में जिस्म
ख़ाक में लिथड़े हुये ख़ून में नहलाये हुये
जिस्म निकले हुये अमराज़ के तन्नूरों से
पीप बहती हुई गलते हुये नासूरों से
लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजे
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मग़र क्या कीजे
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा
राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा
मुझ से पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न माँग
फ़ैज़ की एक और मशहूर ग़ज़ल
गो सबको बहम साग़रो-बाद तो नहीं था
ये शह्री उदास इतना ज़ियादा तो नहीं था
गलियों में फिरा करते थे दो-चार दिवाने
हर शख़्स का सद-चाक-लबादा तो नहीं था
मंज़िल को न पहचाने रहे-इश्क़ का राही
नादाँ ही सही, इतना भी सादा तो नहीं था
थककर यूँ ही पल-भर के लिए आँख लगी थी
सोकर ही न उट्ठें ये इरादा तो नहीं था।