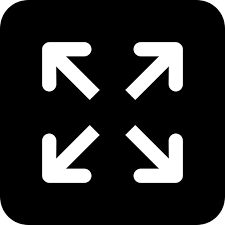शिक्षा के बढ़ते दबाव मे गुम होता बचपन -डॉ. मनीष पाण्डेय
हर परिस्थिति में अव्वल रहने के दबाव के बीच कई लाख की संख्या में विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा पास की| इनके अपनी मानसिक उलझनों के अलावा देश के नीति-नियंताओं के माथे पर भी बल आ गया होगा कि युवाओं की तैयार हो रही इतनी बड़ी फ़ौज को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, जबकि रोज़गार पैदा होने की दर एकदम से घटी हुई है| प्राचीन आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के जीवन को बहुत सीधे सीधे चार चरणों में बाँट दिया गया था जिसमें से प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य यानी पढ़ाई-लिखाई के लिए आरक्षित था| वास्तविकता में यह था या नही, लेकिन सैद्धांतिक रूपरेखा में प्राचीन व्यवस्था काफी सशक्त थी| वर्तमान व्यवस्था में तमाम नियोजित कार्यक्रमों के बाद भी सबकुछ अनिश्चित और अनियमित है| कहा जाता है कि शिक्षा से जीने की वजह मिलती जाती है,लेकिन इसकी भी एक सीमा रेखा है, जिसके आगे के चरण में सबकुछ गड्डमड्ड है| बड़ी विडम्बना यह भी है कि शिक्षा अपने आप मे ही असमानता की बड़ी वजह है| आर्थिक हैसियत के आधार पर ख़रीदी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में छोटी सी चूक भी औरों से कहीं पीछे छोड़ सकती है और इस परिस्थिति का दबाव बच्चों पर सीधे पड़ता है| परिवारिक और सामाजिक संरचना के दबाव के परिणामस्वरूप बच्चे मनोविकार से जूझ रहे हैं| भारी-भरकम पाठ्यक्रम, गालाकाट प्रतिस्पर्धा, परिवार की महत्वाकांक्षा का दबाव, बस्ते का बढ़ता बोझ, खचाखच भरी स्कूल बसों से होने वाला चिड़चिड़ापन, स्वयं को सबसे बेहतर बनाने की प्रवृत्ति, होमवर्क का तनाव, तकनीकी का बढ़ता प्रयोग और यहाँ तक की छुट्टियों में भी खुद को अपडेट रखने की बढ़ती प्रवृत्ति ने बचपने और उनकी मानवीय संवेदना को कमजोर कर दिया है| यह तनाव आगे चलकर और भी जटिल हो जाता है जब तमाम झंझावतों को पार करने के बाद भी रोज़गार और स्थायी भविष्य का भ्रम टूटने लगता है|
इस परिस्थिति के लिए न सिर्फ अभिभावक बल्कि हमारी सामाजिक-आर्थिक संरचना भी जिम्मेदार है| शिक्षा आज के वक़्त बहुत बड़ा और सुरक्षित व्यावसाय है| आज के समाज में ज्ञान ही शक्ति है| जिसके पास विशेष ज्ञान होगा, उसी के पास संसाधन और शक्ति होगी, और यही स्थिति ज्ञान प्राप्ति को प्रदत्त कर आरक्षित कर देती है| इस स्थिति में सीमित संसाधनों पर अपनी हिस्सेदारी को लेकर तनाव बढ़ा है और इसका सीधा शिकार बचपन हो रहा है| अमेरिका के मियामी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अनुमान किया है कि 1970 के बाद पढ़ाई के मानदंड में बढ़ोत्तरी होने का साथ ही ध्यान केन्द्रित नहीं करने के मनोविकार में काफी वृद्धि हुई है| इस शोध से पता चला कि प्री-प्राइमरी में नामांकन तेजी से बढ़ा है और इस वजह से पिछले 40 सालो में ध्यान केन्द्रित न करने के मनोविकार में दोगुनी बढ़ोत्तरी हुई है| मियामी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी पी. ब्रोस्को ने इस अध्ययन में पाया कि 70 के दशक की तुलना में अब बच्चे अकादमिक गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं| हमे लगता है कि पढ़ाई के बोझ से कम उम्र बच्चों के एक वर्ग पर नकारात्मक असर पड़ रहा है| उन्हे आराम और खेल-कूद का वक़्त ही नही मिल पा रहा है| इससे कुछ बच्चों में ध्यान केन्द्रित ना कर पाने का मनोविकार पैदा हो जा रहा है| प्री-नर्सरी स्कूलों में समय से पहले दाखिला दिला देने से बच्चों के व्यवहार संबंधी परेशानियों की संभावना दोगुनी बढ़ जाती है| ख़ैर भारत में इस तरह के अध्ययन ना तो होते हैं, ना ही उनका कोई मतलब है| सान 1992 में बच्चों पर अनावश्यक पाठ्यक्रमों और बस्ते के बढ़ते बोझ को लेकर बनी यशपाल समिति ने स्कूली शिक्षा पर कई सवालिया निशान खड़ा किया और बाद में बने चर्चित ज्ञान आयोग के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं हुआ| शिक्षा का अंध, अनैतिक, अनियंत्रित निजीकरण लगातार जारी है| वैश्वीकरण के इस दौर में निजीकरण को ही एकमात्र विकल्प मान लिया गया है| हालांकि कुछ बैगलेस स्कूलों की अवधारणा ने ज़ोर पकड़ा है लेकिन वह बहुतों के आर्थिक दायरे से बाहर है| बाक़ी हालात ये है कि सरकारें और निजी संस्थान सारा ज्ञान बच्चे के बस्ते में ही ठूंसना चाहते हैं| जबकि मुहावरा सबको पता है कि “ मूर्खों का ही बस्ता सबसे ज्यादा भारी होता है”| आज इसका उल्टा सच बनाया जा रहा है| समान शिक्षा पर चर्चा बेमानी हो रही है, तो क्या समान पाठ्यक्रम पर बात नहीं हो सकती! क्यों ना यथासंभव कक्षा तक की शिक्षा के न सिर्फ़ सिलेबस बल्कि करीकुलम को ही एक समान कर दिया जाए? जिससे हर बच्चा एक समान ज्ञान प्राप्त करे भले ही माहौल और एक्सेसरीज़ अलग हों|
आज बच्चे का सर्वगुण संपन्न होना अनिवार्य आवश्यकता हो गई है| बच्चों से सभी क्षेत्रों मे महारत हासिल करने की अपेक्षा की जाती है| बच्चों पर यह दबाव लगभग सभी वर्ग के अभिभावकों का है| उनको उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों में उन्हे कुछ हासिल करने और योग्यता को लगातार प्रमाणित करने का दबाव छिपा रहता है| यानी व्यावसायिकता अब खून के रिश्तों मे भी अपनी पैठ बना चुकी है| ये बचपन किसी उच्च पद या गौरव की आकांक्षा को सामने रख जुट जाता है, अथक प्रयासों के साथ बिना यह जाने कि उसकी अपनी योग्यता, क्षमता या अरमान क्या हैं? ये बचपन कब अपने मन की भावनाओं और किलकती उमंगों का दमन करते हुए, पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारियों का बोझ लादे इस नई सामाजिक- आर्थिक संरचना मे बेबस बालक से किशोर और किशोर से युवा हो जाता है, पता ही नहीं चलता| इस उच्च उपभोक्तावादी समाज वीभत्स फैलाव के बीच अपने वजूद को ढूँढने की छटपटाहट में जूझते बच्चों को की सुध हम ले भी तो नहीं सकते! क्या समाज की आर्थिक संरचना ही हमारे जीवन और मूल्य को तय नहीं कर रही है?
इस परिस्थिति के लिए न सिर्फ अभिभावक बल्कि हमारी सामाजिक-आर्थिक संरचना भी जिम्मेदार है| शिक्षा आज के वक़्त बहुत बड़ा और सुरक्षित व्यावसाय है| आज के समाज में ज्ञान ही शक्ति है| जिसके पास विशेष ज्ञान होगा, उसी के पास संसाधन और शक्ति होगी, और यही स्थिति ज्ञान प्राप्ति को प्रदत्त कर आरक्षित कर देती है| इस स्थिति में सीमित संसाधनों पर अपनी हिस्सेदारी को लेकर तनाव बढ़ा है और इसका सीधा शिकार बचपन हो रहा है| अमेरिका के मियामी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अनुमान किया है कि 1970 के बाद पढ़ाई के मानदंड में बढ़ोत्तरी होने का साथ ही ध्यान केन्द्रित नहीं करने के मनोविकार में काफी वृद्धि हुई है| इस शोध से पता चला कि प्री-प्राइमरी में नामांकन तेजी से बढ़ा है और इस वजह से पिछले 40 सालो में ध्यान केन्द्रित न करने के मनोविकार में दोगुनी बढ़ोत्तरी हुई है| मियामी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी पी. ब्रोस्को ने इस अध्ययन में पाया कि 70 के दशक की तुलना में अब बच्चे अकादमिक गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं| हमे लगता है कि पढ़ाई के बोझ से कम उम्र बच्चों के एक वर्ग पर नकारात्मक असर पड़ रहा है| उन्हे आराम और खेल-कूद का वक़्त ही नही मिल पा रहा है| इससे कुछ बच्चों में ध्यान केन्द्रित ना कर पाने का मनोविकार पैदा हो जा रहा है| प्री-नर्सरी स्कूलों में समय से पहले दाखिला दिला देने से बच्चों के व्यवहार संबंधी परेशानियों की संभावना दोगुनी बढ़ जाती है| ख़ैर भारत में इस तरह के अध्ययन ना तो होते हैं, ना ही उनका कोई मतलब है| सान 1992 में बच्चों पर अनावश्यक पाठ्यक्रमों और बस्ते के बढ़ते बोझ को लेकर बनी यशपाल समिति ने स्कूली शिक्षा पर कई सवालिया निशान खड़ा किया और बाद में बने चर्चित ज्ञान आयोग के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं हुआ| शिक्षा का अंध, अनैतिक, अनियंत्रित निजीकरण लगातार जारी है| वैश्वीकरण के इस दौर में निजीकरण को ही एकमात्र विकल्प मान लिया गया है| हालांकि कुछ बैगलेस स्कूलों की अवधारणा ने ज़ोर पकड़ा है लेकिन वह बहुतों के आर्थिक दायरे से बाहर है| बाक़ी हालात ये है कि सरकारें और निजी संस्थान सारा ज्ञान बच्चे के बस्ते में ही ठूंसना चाहते हैं| जबकि मुहावरा सबको पता है कि “ मूर्खों का ही बस्ता सबसे ज्यादा भारी होता है”| आज इसका उल्टा सच बनाया जा रहा है| समान शिक्षा पर चर्चा बेमानी हो रही है, तो क्या समान पाठ्यक्रम पर बात नहीं हो सकती! क्यों ना यथासंभव कक्षा तक की शिक्षा के न सिर्फ़ सिलेबस बल्कि करीकुलम को ही एक समान कर दिया जाए? जिससे हर बच्चा एक समान ज्ञान प्राप्त करे भले ही माहौल और एक्सेसरीज़ अलग हों|
आज बच्चे का सर्वगुण संपन्न होना अनिवार्य आवश्यकता हो गई है| बच्चों से सभी क्षेत्रों मे महारत हासिल करने की अपेक्षा की जाती है| बच्चों पर यह दबाव लगभग सभी वर्ग के अभिभावकों का है| उनको उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों में उन्हे कुछ हासिल करने और योग्यता को लगातार प्रमाणित करने का दबाव छिपा रहता है| यानी व्यावसायिकता अब खून के रिश्तों मे भी अपनी पैठ बना चुकी है| ये बचपन किसी उच्च पद या गौरव की आकांक्षा को सामने रख जुट जाता है, अथक प्रयासों के साथ बिना यह जाने कि उसकी अपनी योग्यता, क्षमता या अरमान क्या हैं? ये बचपन कब अपने मन की भावनाओं और किलकती उमंगों का दमन करते हुए, पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारियों का बोझ लादे इस नई सामाजिक- आर्थिक संरचना मे बेबस बालक से किशोर और किशोर से युवा हो जाता है, पता ही नहीं चलता| इस उच्च उपभोक्तावादी समाज वीभत्स फैलाव के बीच अपने वजूद को ढूँढने की छटपटाहट में जूझते बच्चों को की सुध हम ले भी तो नहीं सकते! क्या समाज की आर्थिक संरचना ही हमारे जीवन और मूल्य को तय नहीं कर रही है?
Next Story